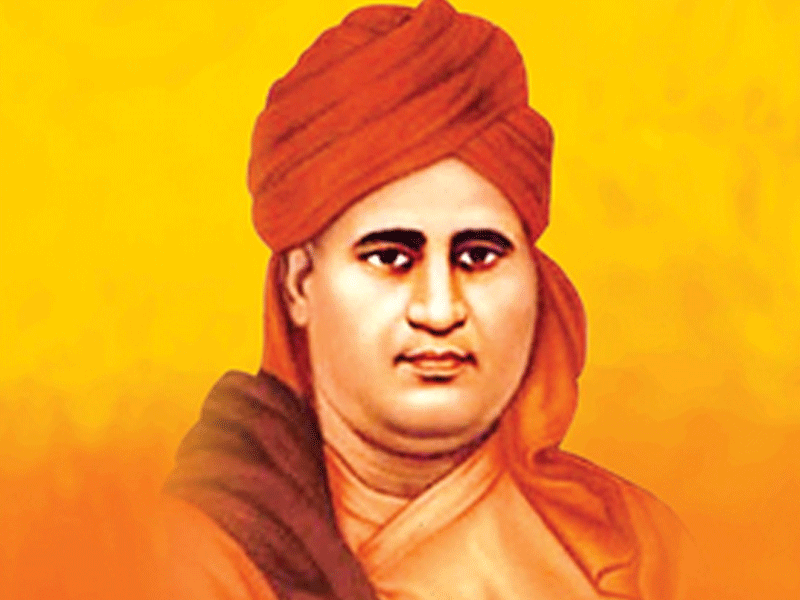गुजरात में काठियावाड़ के मोरबी जिले के अन्तर्गत टंकारा एक ग्राम है। यहां श्री कर्षन जी के यहां एक बालक पैदा हुआ था, यह दिन था 12 फरवरी 1824 ई का पुण्य दिवस है। जिसका नाम रखा गया मूलशंकर। पांच वर्ष की अवस्था में बालक मूलशंकर को अक्षर बोध कराया गया। शीघ्र ही बहुत से वेद मंत्र भी कण्ठस्थ कराये गये। आठवें वर्ष उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर उसे नियम पूर्वक वेद पढ़ाया जाने लगा। चौदहवें वर्ष में उसने व्याकरण, सम्पूर्ण यजुर्वेद और दूसरे वेदों के कुछ भाग याद किया। अब उसे विद्या का स्वाद लग चुका था।
सन् 1838 की शिवरात्रि थी। बालक मूलशंकर के हृदय में शिवजी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। यह उसका पहला व्रत और जागरण करने की। साथ ही भगवान को प्रसन्न करने का सुलभ अवसर था। वह अपने पिताजी के साथ पास के ही एक शिव मन्दिर में गया। वहां बहुत सारे भजन हुए, बाजे बजे, पूजा हुई, ठंडाई बटी, भांग उड़ी। जब रात अधिक होने लगी तो एक-एक करके सभी सोने लगे। अकेला मूलशंकर निद्रा के साथ निरन्तर युद्ध कर रहा था। इतने में एक विचित्र घटना घटी। देखता क्या है कि एक चूहे ने शिवजी पर चढ़ाई की और खूब लूट-मार मचाई।

बालक मूलशंकर को आश्चर्य हुआ। मन में शंका उत्पन्न हुई। तीक्ष्ण – बुद्धि बालक को कोई समाधान नहीं हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा… जब यह सच्चे शिवजी नहीं है तो मैं क्यों व्रत रखूं और क्यों जागरण करूं? मुझे तो सच्चे शिवजी की खोज करनी चाहिए। चूहे की चढ़ाई और 14 वर्षीय भगिनी और फिर चाचा की हैजे से मृत्यु से बालक मूलशंकर को बड़ा दुख हुआ। अपनों को काल के गाल से समाता देख वह अत्यंत दु:खी हुआ। मन कहीं लगता न था। जो भी विद्वान और पण्डित मिलता, उनसे सच्चे शिवजी का पता और मृत्यु को जीतने के उपाय पूछता।
Also Read-
मूलशंकर में वैराग्य की मात्रा बढ़ रही थी और उसके माता-पिता ने इसे विवाह बन्धन में बांधना चाहा। मूलशंकर था बड़ा सयाना। वह इस बन्धन को ही मृत्यु समझता था। अन्त में एक दिन सांयकाल को वह घर से निकल ही पड़ा। उस समय उसकी आयु 21 वर्ष की थी। मूलशंकर ने सुन रखा था कि योग द्वारा सच्चे शिवजी के दर्शन होते हैं, मृत्यु को जीत सकते हैं। अतः घर से निकलते ही उसने सच्चे योगी की खोज आरम्भ की। उसने लगातार साधु, संतों और योगियों के संगत करके देखा और दो वर्ष बाद स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती जी से मूलशंकर ने संन्यास की दीक्षा ली और स्वामी दयानन्द सरस्वती कहलाने लगे।
यहां से मूलशंकर अब स्वामी दयानन्द सरस्वती हो गये। स्वामी जी ने निरन्तर 12 वर्षों तक तीर्थ स्थानों, गुफाओं, जंगलों और पहाड़ों में योगियों की खोज की। तुंगनाथ के ऊंचे शिखर पर और हिमाच्छादित प्रसिद्ध अलकनन्दा पर तक चढ़कर देखा, कहीं सच्चा योगी नहीं मिला। फिर स्वामी जी नीचे उतरकर घूमते – फिरते स्वामी विरजानंद सरस्वती जी का नाम सुन मथुरा पहुंचे। उनकी बाह्य आंखें तो बन्द थीं, पर ज्ञानचक्षु खुले थे। वह केवल ऋषि प्रणीत ग्रंथों पर विश्वास करते थे। उनकी स्मृति बड़ी विलक्षण थी। एक बार सुनने से ही पाठ कण्ठ हो जाता था। उनका पाण्डित्य, उनकी प्रतिभा, उनका शास्त्र ज्ञान, उनका भाषण – चातुर्य सब कुछ अद्भुत था। सारे शास्त्र उनकी जिह्वा पर नाचते थे।
स्वामी दयानन्द सरस्वती तीन चार वर्षो में ही पाणिनीय व्याकरण, महाभाष्य, उपनिषद, मनुस्मृति, ब्रह्मसूत्र, पतंजलि – योगसूत्र, वेद और वेदांगों का पाठ कर गुरु विरजानन्द सरस्वती से दीक्षा लेते हैं। दीक्षांत के समय स्वामी जी गुरु – चरणों में लौंग भेंट करते हैं। गुरु अप्रसन्न होकर कहते हैं, “बेटा ! मैं तुम्हारी लोगों से सन्तुष्ट नहीं हूं। मुझे बहुत कुछ चाहिए। उसके मिलने की आशा तुम्हीं से है। संसार वेदों को भूल चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम संसार में वेदों का सच्चा ज्ञान फैलाओ।”
स्वामी जी ने विनम्र भाव से निवेदन किया- “परम पूजनीय गुरुवर ! दयानन्द अपने तन – मन को अर्पण करता है। ईश्वर आपका एक – एक अक्षर साकार करे।” फिर गुरु चरणों में शीशधर स्वामी जी ने आशीर्वाद मांगा। गुरुवर प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देकर शिष्य को विदा करते हैं। उस समय दयानन्द की आयु 39 वर्ष की थी। गुरुवर के आशीर्वाद को लेकर स्वामीजी आगरा, ग्वालियर, जयपुर, अजमेर आदि स्थानों में पहुंचकर अनेक सम्प्रदायों के साथ तर्क – युद्ध करने लगे। इस युद्ध में यूं तो विजय स्वामीजी की ही होती रही, पर मन में शंकाएं भी कईं प्रकार की उत्पन्न होती रहीं। अपने मूल सिद्धान्तों को निश्चित करने और शंकाओं का समाधान पाने स्वामीजी सन् 1867 में फिर गुरु चरणों में उपस्थित हुए। स्वामीजी की अपने गुरु से यह आखिरी भेंट थी।
महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सन् 1867 में कुम्भ के मेले हरिद्वार पहुंचे, यहां पर एक ऊंचा स्थान पर्णकुटी में “पाखण्ड मर्दन” नाम का पताका लगा, सारे अवैदिक मतों का तीव्र खण्डन किया। साथ ही शुद्ध वैदिक धर्म का उपदेश भी दिया। कुम्भ के मेले से चलकर स्वामीजी फर्रुखाबाद पहुंचे। वहां स्वामीजी ने मूर्ति पूजा का इतना घोर खण्डन किया कि लोग उन्हें मारने का षड्यन्त्र रचने लगे। स्वामीजी का ओजपूर्ण और तत्व – सम्पन्न खंण्डन सुन असंख्य मूर्तिपूजकों ने अपनी – अपनी मूर्तियां गंगाजी में बहा दीं।
स्वामीजी काशी पहुंचे। यहां मंगलवार 17 नवंबर सन् 1869 को 3 बजे शास्त्रार्थ का समय निश्चित हुआ। विपक्षियों में पण्डित ताराचरण तर्करत्न, स्वामी विशुद्धानन्द, पण्डित बालशास्त्री आदि शास्त्रार्थ महारथी आगुवा थे। काशी नरेश इस सभा के अध्यक्ष थे। इस शास्त्रार्थ के विषय में ‘हिंदू पेट्रियट’ के 17 जनवरी 1870 के अंक में इस शास्त्रार्थ का उल्लेख निम्न प्रकार दिया गया है – “… दयानन्द सरस्वती और पण्डितों में बड़ा भारी और लम्बा शास्त्रार्थ हुआ। परन्तु पण्डितों का, जिन्हें अपनी शास्त्रज्ञता का गर्व था, पूर्ण पराजय हुआ। पण्डितों ने जब जान लिया कि नियमबद्ध शास्त्रार्थ में ऐसे महान व्यक्ति से पार पाना असम्भव है तो वह अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए पापमय उपायों के अवलम्बन पर उतारू हो गये।…” काशी के इस शास्त्रार्थ से देश के कोने-कोने में वेद का सन्देश पहुंचा। अगले चार मास तक स्वामीजी यहीं रहे। मूर्तिपूजा का और भी तीव्र खण्डन करने लगे पर किसी की हिम्मत स्वामीजी के सामने आने की न हुई। इस शास्त्रार्थ से ऋषि को पता चला कि और तो और स्वयं काशी का पण्डितवर्ग भी सच्चे ईश्वर और सत्य मार्ग से कितनी दूरी पर है।
स्वामीजी ने भारतवर्ष में अनेकों स्थानों में शास्त्रार्थ करके वहां के पण्डितों को परास्त किया। इन शास्त्रार्थों और व्याख्यानों का देश पर अच्छा प्रभाव पड़ा। सहस्त्रों व्यक्ति वेदों के भक्त बन गये। अतः स्वामीजी ने अनेकों स्थानों में “वैदिक पाठशालाएं” खोलना आरंभ किया। इन पाठशालाओं के लिए जो अध्यापक मिले थे, उनके हृदयों में से पुराणों की गहरी छाप अभी निकली न थी। यह देख स्वामीजी ने इन पाठशालाओं को तुरन्त ही बन्द कर दिया। स्वामीजी वेद प्रचार कार्य को स्थिर बनाये रखना चाहते थे। इसी उद्देश्य से आर्यसमाज की स्थापना बुधवार 7 अप्रैल सन् 1875 को मुंबई नगर के गिरगांव में हुई, ऐसा आजकल प्रसिद्ध है। ऋषि बड़े ही अद्भुत और महान थे। उन्होंने सच्चे ईश्वर का अनादर और अपमान न हो, सभी लोग ईश्वर की आज्ञा — वेदमत का पालन करें। समस्त संसार के लोग उस एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें।
वेद जिसे ईश्वर ने मनुष्यों को सृष्टि के आदिकाल में दिया। इसमें मनुष्यों के सारे कर्तव्य आ जाते हैं। समस्त सत्य विद्या का आदि मूल वेद है। लोग प्रभु की वाणी इस वेद को भूल चुके थे। आर्य भाषा में इसका भाष्य सबसे पहले ऋषि दयानन्द ने ही किया ताकि साधारण बुद्धिवाला प्रत्येक मनुष्य पढ़कर अपना जीवन सुधार सकें। पहले तो वेद यहां पर प्रकाशित ही नहीं हुए थे। जर्मनी से ऋषि ने ही वेद मंगाये थे। फिर वैदिक यन्त्रालय खोलकर वेदभाष्य छपवाना आरम्भ किया। फिर अपना भाष्य संसार के सामने रखकर सबको वेद की प्रधानता का पाठ पढ़ाया। आर्यसमाज ने ऋषि के इस वेद प्रचार को ही अपना मुख्य कार्य बनाया और यह है भी मुख्य।
संदर्भ ग्रंथ : महर्षि चरित्र प्रकाश
लेखक : भक्त राम
अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी पंडित गंगाराम स्मारक मंच, हैदराबाद
मोबाइल नंबर- 98490 95 150