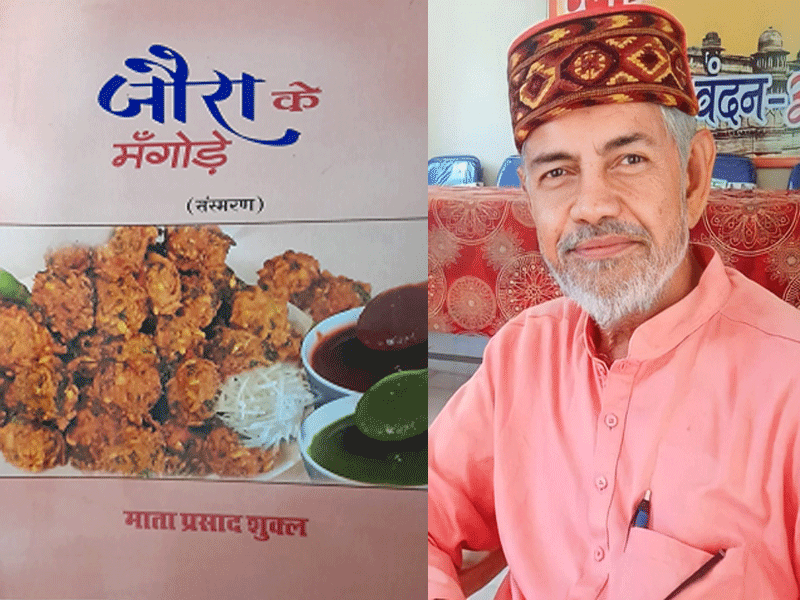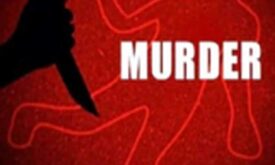माता प्रसाद शुक्ल के द्वारा लिखित ‘जौरा के मंगोड़े’ नामक संस्मरणात्मक पुस्तक का प्रथम संस्करण सन् 2022 में कानपुर से प्रकाशित हुआ था। तत्पश्चात द्वितीय संस्करण का प्रकाशन सन् 2023 में हुआ। ग्वालियर के इतिहासकार माता प्रसाद शुक्ल ने प्रस्तुत पुस्तक में सम्मिलित कुल 41 संस्मरणों में अपने देखे-भोगे समकाल की रोचक स्मृतियों को विस्तार से सँजोया है। इन संस्मरणों में उन्होंने राजनीतिज्ञ से लेकर स्थान विशेष के भोजन तक को शामिल किया है। इस कारण से प्रस्तुत पुस्तक की पठनीयता और सार्थकता दोगुनी हो चुकी है।
स्मृति के आधार पर किसी विषय, व्यक्ति, स्थान पर लिखित आलेख को ‘संस्मरण’ कहा जाता है। संस्मरण को ‘साहित्यिक निबंध’ कहना भी पूर्णतया गलत नहीं होगा। हिंदी के प्रारम्भिक संस्मरण लेखक के रूप में पद्मसिंह शर्मा का नाम लिया जाता है। इनके अलावा महादेवी वर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। संस्मरण को अंग्रेजी में ‘Memoirs’ कहा जाता है। डॉ. नगेंद्र ने संस्मरण को ‘व्यक्ति का अनुभव तथा स्मृति से रचा गया इतिवृत्त अथवा वर्णन’ कहा है। डॉ. नगेंद्र की परिभाषा के आधार पर यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि संस्मरण में तीन तत्वों का रहना बहुत आवश्यक है- 1. चित्रात्मकता, 2. कथात्मकता और 3. तटस्थता।
माता प्रसाद शुक्ल की लिखित पुस्तक ‘जौरा के मंगोड़े’ संस्मरणात्मक पुस्तक है। इस पुस्तक के साथ मेरा अपना भी संस्मरण अवश्य ही जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी के माध्यम से इस अद्भुत पुस्तक के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। उनके अध्ययन कक्ष में सामने रखी इस पुस्तक के शीर्षक से आकर्षित होकर जब मैंने इसके बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने उत्साहपूर्वक प्रशंसा करते हुए विशेष रूप से इस बात पर ज़ोर दिया कि ‘यह केवल पुस्तक नहीं है ज्ञान और अनुभव का भंडार है’ और समीक्षा लिखने के लिए पुस्तक मुझे थमा दी। साथ ही डॉ. पूर्णिमा शर्मा जी ने ‘मंगोड़े’ बनाने की विधि से अवगत कराया।
यह भी पढ़ें-
प्रस्तुत पुस्तक का पारायण करते हुए माता प्रसाद शुक्ल (जिनके प्रत्यक्ष साक्षात्कार का अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है) की विचारधारा को कमोबेश पढ़ने-जानने का सुअवसर मिला। ‘याद’ या ‘संस्मरण’ केवल शब्द नहीं हैं, इन शब्दों के साथ जीवन के ‘अनुभव’ जुड़े हुए होते हैं। ये याद और अनुभव साधारण से लेकर अति विशेष किसी भी प्रकार के व्यक्ति के कारण से प्राप्त हो सकते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने ऐसे अनेक व्यक्तियों को याद किया है जिनके कारण से लेखक को संस्मरणात्मक पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली है। उनके संस्मरण इस कारण से भी विशेष बन गए हैं क्योंकि उन यादों और अनुभवों के द्वारा अवश्य ही पाठकों को नवीन सूचना मिल रही है। जैसे जब उन्होंने ग्वालियर रियासत की अंतिम महारानी श्रीमंत विजया राजे सिंधिया और हर दिल अज़ीज माधवराव सिंधिया के बारे में संस्मरण लिखा तो केवल उन व्यक्तियों के बारे में ही नहीं लिखा, उनके संस्मरण के द्वारा दक्षिण में, तेलंगाना में, बैठी मुझ जैसी एक आम पाठक को ग्वालियर के इतिहास को जानने का अवसर मिला, जिसे यही लगता था कि गणेश उत्सव तो महाराष्ट्र के बाद भाग्यनगर यानी हमारे हैदराबाद में ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन रोचक जानकारी यह भी है कि ‘ग्वालियर में तीन दशक पूर्व गणेश उत्सव के समय बाज़ारों और मोहल्लों में झाँकियाँ लगाने की परंपरा थी। जो अब लुप्तप्राय: होती जा रही है। एक बार शिंदे की छावनी में, जो राजमहल जयविलास पैलेस के नजदीक ही एक बस्ती और बाज़ार हुआ करता है। सन् 1981 में इन पंक्तियों के लेखक ने तीनदिवसीय झाँकियों का आयोजन जन सहयोग से किया। उस अवसर पर झाँकियों की प्रतियोगिता होती थीं। सर्वश्रेष्ठ झाँकियों को पुरस्कार और सम्मान पत्र दिए जाते थे’। 1
साथ ही साथ यह भी जानना रोचक लगा कि ‘सन् 1947 में वतन को आजादी मिल गई। देश के राजे-रजवाड़े क्रमश: समाप्त होते गए। लेकिन ग्वालियर के महाराज हमेशा महाराज ही रहे, क्योंकि वे लोगों के आम जन सर्वहारा के दिलों में राज करते थे। वे हर दिल अजीज थे। देश के अन्य नेताओं की तरह महाराज किसी जाति अथवा वर्ग और नस्ल तक ही सीमित नहीं रहे। उनका प्रभाव सम्मान और आदर सभी क़ौमों में था। यही कारण है कि वे कभी चुनाव में पराजित नहीं हुए, उन्होंने लाखों मतों से विजय श्री को वरण किया’। 2
आज के वर्तमान भारत में जब एक देश एक चुनाव, आरक्षण विहीन देश आदि मुद्दों पर बहस और चर्चा होती रहती है, उस समय शुक्ल जी का संस्मरण केवल स्मृतिचारण नहीं रह गया है, बल्कि देश की जनता राजा से क्या चाहती है? इसका उत्तर बन चुका है। संस्मरण के तत्वों पर चर्चा करते समय चित्रात्मकता को इसके एक प्रमुख गुण के रूप में पाया गया है। चित्रात्मकता इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि संस्मरण याद और अनुभव दोनों को एक साथ लेकर चलता है। अनुभव अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का हो सकता है। अच्छे अनुभव तो फिर भी व्यक्त हो जाते हैं, लेकिन बुरे अनुभवों को वर्णित करने के लिए भावना की ईमानदारी, तटस्थता और भाषा की सजीवता का होना बहुत आवश्यक है। माता प्रसाद शुक्ल जी की पुस्तक ‘जौरा के मंगोड़े’ में इन विशेषताओं को चित्रात्मक शैली में समाहित देखा जा सकता है। ‘मेरे प्रेरणा स्रोत एक नहीं अनेक’ संस्मरण में उनके द्वारा लिखित कुछ शेर पढ़ने को को मिले हैं–
‘रोज आते रहो रोज जाते रहो।
उम्र भर यूँ ही तुम मुस्कराते रहो।
अभी उसकी आस बाकी है।
होठों की मिठास बाकी है।
यूँ ही कातिल निगाहों से न देखा कीजिए।
आप मेरी नियत को न खराब कीजिए’। 3
ये शेर अपने आप में लाजवाब तो हैं ही, साथ ही लेखक की स्वीकारोक्ति कि ‘मैं उन सभी ज्ञात और अज्ञात मोहतरमाओं का ऋणी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मैं थोड़ा दिलफेंक आदमी रहा हूँ। अभी भी मेरे पास प्रेरणाओं की कमी नहीं। खुदा का शुक्रिया। … अब मैं अपनी स्थायी प्रेरणा स्रोत का जिक्र कर रहा हूँ, वो है मेरी धर्मपत्नी महादेवी। ये महिला अगर मेरे जीवन में न आई होती तो मैं लेखक या रचनाकार कदापि नहीं होता’। जैसे संवाद पुस्तक को रोचक बना देती है। 4
ग्वालियर को पत्थरों का शहर कहा जाता है और इसे गीतों की नगरी भी कहा जाता है। इस शहर के राजे-रजवाड़ों को तो सब पहचानते हैं। लेकिन दुखद सत्य यह भी है कि राजनैतिक रूप से कम्युनिस्ट विचारधारा को माननेवाले, फ़कीराना स्वभाव के व्यक्ति प्रसिद्ध संगीतकार बैजू कानूनगो को आज भी संपूर्ण भारत नहीं जानता है। जबकि, ‘वे ग्वालियर के राजदूत थे। उन्होंने अपने शहर की प्रतिष्ठा अपनी मेहनत, अपने सफल संचालन के कारण पूरे देश में बढ़ाई। जब कोई शख्स अपने शहर से बाहर जाता है तो वह अकेला नहीं जाता है। वह अपने शहर की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों एवं अपनी भाषा को साथ लेकर जाता है। उसके व्यवहार और आचरण ही उसके शहर की नुमाइंदगी करते हैं। बैजू दादा ने अपने आचरण और व्यवहार से अपने शहर ग्वालियर की आन-बान-शान की परंपरा को शिखर पर पहुंचाया था’। 5
ऐसे व्यक्ति के साथ बात करते समय किस कारण से दुख का अनुभव हुआ था!? इसे ही याद करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, ‘पिछले वर्ष बैजू दादा ने मुझे फोन पर बसंत ऋतु पर चार दोहे सुनाए थे, बस यही मलाल है कि उनका कोई संग्रह जनता के बीच नहीं आ सका। हमने उनसे कहा था कि हम आपका संग्रह साहित्यकार कल्याण ट्रस्ट की ओर से प्रकाशित कराए देते हैं, तब उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी पांडुलिपि चंबल में फेंक जाऊँगा’। 6
यहीं पर आकर संस्मरणात्मक पुस्तक की आवश्यकता और महत्ता बढ़ जाती है। लेखक ने पाठकों के सामने बैजू दादा द्वारा रचित निम्न रचना को पढ़ने का अवसर देकर किताब की प्रासंगिकता को नवीन आयाम प्रदान कर दिया है-
‘स्वागत में रितुराज के, प्रकृति हुई तल्लीन।
फूलों के तोरण सजे, पत्तों के कालीन॥
पतझर को देकर विदा, लौटा संत बसंत
रोम-रोम पुलकित हुआ, जिसका आदि न अंत’ 7
जीवन पथ की यात्रा करते समय हम ऐसे अनेक लोगों से मिलते हैं, जिनकी कहानी हमें बैजू दादा की कहानी से मेल खाती हुई दिखाई पड़ती है; तो हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो श्री कृष्ण चंद्र तिवारी के समान कर्मयोगी बनकर डॉ. राष्ट्रबंधु की उपाधि से भी सम्मानित होते हैं। ऐसे महान लोग मानवता के ऊपर आस्था बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ माता प्रसाद शुक्ल जी फतेहगढ़ साहेब गुरुद्वारा गए थे। उनकी यात्रा का विवरण पाठकों को फिर से इस सत्य से अवगत कराता है कि ‘हिंदू धर्म आज सिक्खों के त्याग और गुरुओं की बलिदानी परंपरा के कारण ही जिंदा है। वरना यह देश मुगल सल्तनत में ही मुगलस्तान हो जाता। हिंदू धर्म के अनुयायी सिक्खों के ऋणी हैं, ऋणी होना ही चाहिए’। 8
शुक्ल जी के इस वक्तव्य ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि उन्हें अपने देश के इतिहास, संस्कृति, सभ्यता का पूर्णरूपेण ज्ञान है और साथ ही वे अपनी भारतीय पहचान पर गर्वित भी हैं। राष्ट्रबंधु क्यों राष्ट्रबंधु नाम से जाने जाते थे। इसका भी ज्ञान शुक्ल जी के संस्मरण से होता है। 2 अक्तूबर 1933 को शाहजहाँपुर (उत्तर प्रदेश) में जन्मे राष्ट्रबंधु का मूल नाम श्री कृष्ण चंद्र तिवारी था। राष्ट्रबंधु उनका उपनाम था। वे सारे देश में अपने उपनाम से ही जाने जाते थे। मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बाल साहित्य में पीएचडी की थी। वे मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग में थे। राष्ट्रबंधु अनेक शहरों में पदस्थ रहे। सेवानिवृत्त भी इसी विभाग से हुए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा उन्हें पेंशन दी जाती थी। संघर्ष और गरीबी से उनका करीबी नाता रहा’। 9
सोना आग में तपकर ही निखरता है। इसलिए ही वह दूसरे रत्नों को सहज ही स्वीकार कर पाता है। तभी तो ‘ग्वालियर के बाल साहित्यकार थे जगदीश सरीन, जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त थे। दैवयोग से श्री सरीन को गले का कैंसर हो गया था। उनके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। स्थानीय स्तर पर भी ग्वालियर वासी उनका सहयोग कर रहे थे। उन दिनों डॉ. राष्ट्रबंधु कानपुर के साहित्यकारों की ओर से पाँच सौ रुपए की धनराशि जगदीश सरीन को भेंट करने आए थे’।10
‘आज तो अनेक साहित्यिक संस्थाओं ने इस पवित्र साहित्य कर्म को सेवा के बजाय एक व्यावसायिक रूप दे दिया है। सैंकड़ों ही नहीं, हजारों रुपए एंट्री फीस साहित्य के नाम पर हड़प ली जाती है। स्थानीय स्तर पर भी प्रत्येक शहर में ये संस्थाएँ कुकुरमुत्तों की तरह फैल रही हैं। इनके आयोजकों को न साहित्य का ज्ञान है और न उसकी परंपरा का’।11
ऐसे में धनराशि कितनी है? कौन, किसे, क्या दे रहा है? प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने दर्शाया है कि कैसे यह सब कुछ गौण बन गया है सहकारिता की भावना के सामने। शुक्ल जी ने केवल संस्मरण नहीं लिखा है, उन्होंने वर्तमान साहित्य को उसके अतीत के साथ मिलवाया है और कहीं न कहीं भविष्य में साहित्य ने अगर अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो उसे किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसका भी संकेत दे दिया है।
इस विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हो ही गया है कि संस्मरण लेखक कितने तटस्थ हैं और वे केवल अतीत में जीनेवाले साहित्यकार नहीं हैं बल्कि वर्तमान की उन्हें पुंखानुपुंख जानकारी है। वे वर्तमान और अतीत का तुलनात्मक अध्ययन निरपेक्ष रूप में भी करने को तैयार हैं। संस्मरण केवल अतीत को जीने का नाम नहीं है, बल्कि संस्मरण अवसर देता है अतीत की गलतियों से शिक्षा लेकर व्यक्ति को अपने में सुधार लाने का। जैसा अवसर और ज्ञान प्रोफेसर पृथ्वीराज दुआ जी को मिला। शुक्ल जी ने यादों की पिटारी को खंगालते हुए लिखा है, ‘मैंने अटल जी से हाथ जोड़कर नमस्कार की और उनसे कहा कि ये प्रोफ़ेसर पृथ्वीराज दुआ हैं, कवि हैं, इनका एक कविता संग्रह प्रकाशित हो रहा है। आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, संग्रह पर। दोस्तो! इस बीच दुआ साहब ने एक बेवकूफी कर दी। अपनी जेब से विज़िटिंग कार्ड निकाला और अटल जी को थमा दिया। यह कहकर कि यह मेरा विज़िटिंग कार्ड है। अटल जी ने विज़िटिंग कार्ड तो ले लिया, मगर अटल जी एकदम से उखड़ से गए, बोले हम ऐसे आशीर्वाद नहीं देते। काव्य संग्रह आ जाने दीजिए’। 12 ‘श्रद्धावान लभते ज्ञानम’ क्या यह संस्मरण पाठकों को फिर से याद नहीं दिला रहा है?
निष्कर्षतः, शुक्ल जी ने अपने जीवन को पूरी संसक्ति के साथ जिया है और उनके संस्मरण सभी वर्ग के पाठकों को मनोरंजन, ज्ञान, रोचकता आदि प्रदान करने में सक्षम है।
समीक्षित पुस्तक:
जौरा के मंगोड़े (संस्मरण)
लेखक-माता प्रसाद शुक्ल
प्रकाशन- श्री नर्मदा प्रकाशन
ISBN-978-93-96268-54-6
संस्करण-द्वितीय-2023
मूल्य-300/-

समीक्षक: डॉ सुपर्णा मुखर्जी
सहायक प्राध्यापक
भवंस विवेकानंद कॉलेज
सैनिकपुरी, हैदराबाद- 500094 drsuparna.mukherjee.81@gmail.com