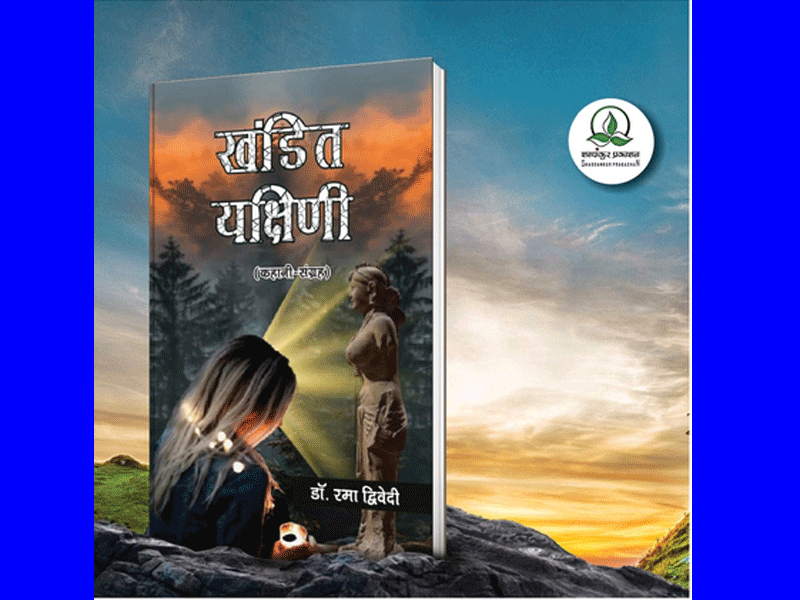मूल्यों के टूटन और विघटन से उत्पन्न सामाजिक द्वंद्व की स्थिति से व्यथित हृदय से उत्पन्न उत्तेजित विचार संवेदनाओं में परिवर्तित हो जब चित्र-चरित्र ,नायकों और पात्रों के रूप में विश्वसनीयता के साथ गहरे विचार बद्ध हो, जीवन के अनुभवों की श्रृंखलाओं का गुँथाव महसूस करने लग जाते हैं तो संवेदनशील व्यक्ति स्व और पर के भीतर शिनाख्त कर द्वंद्व की स्थितियाँ महसूस कर, एकदम से छटपटा उठता है और तब इन्हीं द्वंद्वों से मुक्ति की छटपटाहट उसे कथा-कहानियों के सृजन की ओर लिए जाती है। फिर चाहे वह संस्कृति के मूल में परंपराओं के नाम पर बनते-भटकते इतिहास के सामाजिक पन्ने लिखे जाएँ ,या फिर धर्म की आड़ में पितृसत्तात्मक सामंतवाद के अंतर्निहित छले जा रहे अस्तित्व-बोध की गाथा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साक्ष्यों में फॅंसा अद्यतन चिंतन ही क्यों न कलमबद्ध हो! सृजनशील हृदय के भीतर हो रहे द्वंद्वों से मुक्ति की ये छटपटाहट, सृजन के विस्तृत भाव,पन्नों तक की यात्रा की ओर बढ़ ही जाते हैं। डॉ.रमा द्विवेदी का सद्य: प्रकाशित कहानी संग्रह ‘खंडित यक्षिणी’ भी ऐसी ही यात्रा का पड़ाव है। शब्दांकुर प्रकाशन से प्रकाशित 122 पन्नों के इस प्रथम संस्करण में कुल 15 कहानियाँ हैं और ये सभी कहानियाँ अलग-अलग तेवर और कलेवरों में लिखे जाने के बाद भी लेखिका के भीतरी द्वंद्वों की ही अभिव्यक्ति हैं।
अब सवाल उठता है कि द्वंद्वों की मुक्ति की छटपटाहट में लिखी गईं ये कहानियाँ जब कई अलग कलेवरों को प्रदर्शित करती हैं तो फिर इस संग्रह का नाम खंडित यक्षिणी ही क्यों? कहीं ये पौराणिक आख्यानों से उपजी कहानियाँ तो नहीं या फिर यदि पितृसत्तात्मक व्यवस्था से उपजी छटपटाहट हैं तब भी यक्षिणी ही क्यों खंडित के आगे कोई और अन्य विकल्प लेखिका ने क्यों नहीं चुना? आख़िर इसके लिए महादेव की दासियों की यक्षिणी ही क्यों? सत्य है,यक्षिणी शब्द स्त्री-चेतना की आवृत्तियों को बढ़ानेवाला स्त्री-संस्करण से ही रूपायित है। ऐसा संस्करण स्त्री-अस्तित्व की सकारात्मकता को प्रकृति और संरक्षणात्मक शक्ति से जोड़कर उसे एक उर्वर चेतना का रूप देता है। यक्षिणियाँ इस संदर्भ में पितृसत्तात्मक समाज की इस द्वन्द्वात्मक व्यवस्था की भोगवादी प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करने में बहुत सक्षम भी हैं।
यही कारण भी है कि साहित्य में सृजकों ने यदा-कदा इनका चुनाव भी किया है। फिर चाहे दीदारगंज की यक्षिणियों पर लिखी कविताएँ हों या पौराणिक यक्षिणियों की स्त्री-चेतना से सिक्त आनंद उषा बोरकर की कृति यक्षिणी हो या फिर नील डीसिल्वा की अंग्रेजी में लिखी यक्षिणी हो। यक्षिणी अपने कमनीय शरीर के उठान व लोच के सौंदर्य प्रतिमानों के कारण वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित कामुक सौंदर्य सत्ता के प्रतीकों से जहाँ पितृसत्तात्मक समाज की भोगवादी लालसा को जगाती और तृप्त करने का सामर्थ्य रखती हैं वहीं दूसरी ओर सौंदर्य सत्ता के प्रतीकों से ऊपर शक्ति और आत्मचेतना की सशक्त सकारात्मकता का जीवंत पर्याय भी होती हैं। ऐसा पर्याय जो स्त्री के भीतर की रहस्यमयी सत्ता में आत्म विश्वास जगाकर उसे निर्णय लेने के लिए संकल्पित करती है जैसा कि संकलन की शीर्षक कहानी खंडित यक्षिणी में हम देखते भी हैं। प्रेमी से पति बने अपने पति प्रेम को जब प्रिया अपने ब्रेस्ट कैंसर होने की सूचना देती है तो वह जिस तरह इस विपरीत परिस्थिति में उसका संबल बनने के बजाए उससे दूरी बनाकर उसे तोड़ने की कोशिश करता कहता है-
यह भी पढ़ें-
‘‘मैं आकर क्या करूँगा? …
तुम अपना इलाज करवाओ और माँ के पास चली जाओ।’’
ऐसे उत्तर से अवाक हो टूटने और खंडित होने के बाद भी प्रिया अपने भीतर की करिश्माई स्त्री-चेतना को टटोल निर्णय लेती है…
‘‘मैं अपना अस्तित्व इतनी आसानी से कभी मिटने नहीं दूँगी।मैं शक्तिपुंज हूँ। मैं अपने विचारों और अपनी साधना में जीवित रहूँगी।’’
‘‘मैं सिर्फ तुम्हारी प्रेमिका नहीं बल्कि… आदिशक्ति हूँ। मेरा सौंदर्य दीदारगंज की यक्षिणी-सा खंडित ही सही पर मैं युगों-युगों तक अपनी अदम्य जिजीविषा को कभी मिटने नहीं दूँगी।’’
“हाँ! मैं खंडित यक्षिणी हूँ पर अभी तक मैं जिन्दा हूँ और ज़िंदा रहूँगी।”
इन आत्मिक संवादों से मजबूती ले स्वयं को समेटकर खड़े हो, अपने लिए ठोस निर्णय ले ब्रेस्ट कैंसर से अकेली लड़कर जीवन की जीवंत सत्ता में लौटने का फैसला लेना प्रिया के भीतर की उन्हीं रहस्यमयी सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हैं जो यक्षिणियों के भीतर की अदृश्य आध्यात्मिक-आत्मिक सत्ता में उपस्थित होती है। हालांकि प्रेम के व्यवहार से टूटती प्रिया को बार-बार वह पल याद आते हैं जब वह थका-हारा उसके सौंदर्य की कमनीयता के उठान में छिपकर चैन की साँस के लिए बेचैन उनमें छिपा रहता था। इन स्मृतियों को याद कर, भोगवादी पुरुष द्वारा ठगे जाने का अहसास उसे कई बार भीतर से खंडित भी करता है, लेकिन वह उसी भीतर से मिली सकारात्मक ऊर्जा से निर्णय ले अकेली लड़कर जीवन की ओर लौट आती है।
इस संदर्भ में पुरुष समाज का स्वयं का किनारा कर मौन रहना न सिर्फ समय की दहलीज पर खड़े प्रेम के जैविक क्रिया के घृणित रूप को दर्शाता है बल्कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के द्वंद्वों पर कई सवाल भी खड़े करता है। संदर्भगत मुझे उदय प्रकाश जी की कहानी ‘खंडित स्त्रियाँ’ याद आती है जिसमें उन्होंने भी ऐसे प्रश्नों की ओर संकेत करते हुए समाज के अँधेरों में झाँकने की कोशिश की है। यक्षिणियों और स्त्रियों की साम्यता को अनुभूत कहते हैं कि देवता की पूजा सेवा या उसका विराट बोझ ढोने के लिए ही इन पत्थर की स्त्रियों को गढ़ा गया था। सच है, हमारे समाज के भोगी सामंतवादी परिवेश की दृष्टि में स्त्रियाँ ऐसे ही तो गढ़ी गई हैं।
ऐसा नहीं कि लेखिका ने अतिरेकवादी की तरह शीर्षक कहानी की इस स्त्री चेतना को ही संपूर्ण संकलन की कहानियों को केंद्र में रख पुरुष-चेतना की जीवंतता के व्यावहारिक पक्ष को दरकिनार कर रखा है। नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुरुष की भोगवादी प्रवृति के वर्णन की अतिरेकता को मिटाते हुए संकलन की पहली कहानी, ‘पिता की ममता’ में उन आयामों को भी छुआ है जहाँ स्त्री के प्रति पुरुष की संवेदनशीलता और पिता की कर्तव्यनिष्ठा के साथ-साथ स्नेह वात्सल्य के नवीन और सकारात्मक सोच सामने आते हैं और सामाजिक द्वंद्व के घिसे-पिटे स्वरूप का अतिरेक थोड़ा जाता हुआ-सा महसूस होता है..।
कहानी के पात्र डॉक्टर खरे की पत्नी को जब ब्रेस्ट कैंसर डिक्लेयर होता है तो वह सामान्य भोगवादी पुरुषों की तरह, मुँह फेरने के बजाय इस लड़ाई में अपनी पत्नी का साथ देते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं किंतु उसे बचाने की हर संभव कोशिश करने के बाद भी उसे खो देते हैं। बाद में परिस्थितियों के आगे की गई दूसरी शादी में स्वयं की खुशी तलाशने के बावजूद उन्हें यह लगता है कि दूसरी स्त्री उनके बच्चों के लिए उचित नहीं तो वह दूसरी शादी के बाद भी, अपनी खुशी की जगह बच्चों के हक में निर्णय लेना चुनते हैं। इस कहानी से स्पष्ट है, लेखिका ने इस संकलन में, महज स्त्री-विमर्श को ही केंद्र में नहीं रखा है,बल्कि अन्य कहानियों में सामंतवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बात करने के साथ-साथ नवीन परिवेश में हो रहे आंशिक परिवर्तन के तहत पुरुष के भीतर स्त्री के प्रति जागरूक संवेदनाओं को भी सामने रखा है।
सत्य है, सृजन की स्त्री-दृष्टि, खंडित होती स्त्री-चेतना और उसके युगों से जारी आत्म-संघर्षों से उद्वेलित अपने संवेदनशील हृदय को दरकिनार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वह भी तब जबकि यह खंडन, स्त्रियों के आत्म संघर्ष, परंपरा और ऐतिहासिक भौतिकवाद की अभिव्यंजित प्रणालियों की देन हो। जिसमें संस्थागत साजिशों और पितृसत्तात्मक सामंतवादी उद्देश्यों के तहत धर्म और मंदिर संस्कृति की आड़ में पुरुषों द्वारा निर्धारित नीतियों की जगह एक ऐसा षड्यंत्र और बर्बर नियम हो जो स्त्रियों के संपूर्ण अस्तित्व का वस्तुकरण कर, उसकी संपूर्ण स्वायत्तता को जघन्य प्रथा के नाम कर उनके सांस्थानिक शोषण का अधिकार स्वयं ही स्वयं को दे देते हों।
संकलन में शामिल कहानी, ‘आखिरी देवदासी’ स्त्रियों की इन्हीं स्थानिक-यौन-शोषण की बात करती है। हालांकि, देवदासी और देवदासी प्रथा पर साहित्य ने पहले भी दृष्टि डाली है और विस्तृत दृष्टि डाली है। प्रसाद की कहानी देवदासी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है जिसमें वह पत्र लेखन शैली के तहत प्रिय रमेश को संबोधित करते हुए देवदासियों की पीड़ा का चित्रण करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी अपने तरीके से अपनी कहानी देवदासी में इस पीड़ा को दर्शाया है और उनके पहले और बाद भी सृजकों की दृष्टि ने इस प्रथा की जघन्यता को कई बार सामने लाने की कोशिश की है। इसी पीड़ा को भीतर गहरे महसूस करती लेखिका रमा जी की स्त्री-दृष्टि भी अपनी कहानी आखिरी देवदासी में अभिव्यक्त करने की सफल कोशिश की है। अपनी कहानी में एक नन्हीं अबोध बालिका के माध्यम से कहती हैं-
‘‘जब घंटियों की गूँज मौन हो जाती है तब गहरी अँधेरी रात की दीवारों से मैं सुनती रहती अपनी अम्मा की अतृप्त सिसकियाँ। ’’
आगे,11 वर्ष की नन्हीं अवस्था में देवदासी बना दिए जाने के बाद उसकी उम्र से चौगुने उम्र के पुजारी और मठाधीशों द्वारा किये गए यौन शोषण की पीड़ा से बिलबिलाते असहनीय दर्द से टूटती देह और खंडित होती उसकी आत्मा का मार्मिक चित्रण करते उसके संवादों में लेखिका लिखती हैं-
‘‘काली गहरी भयावह उस रात्रि में जब मैं सो रही थी तब मैंने अपने शरीर पर रेंगता लिजलिजा चिपचिपाता-सा हाथ का स्पर्श महसूस किया और आँख खुल गई तब अपने शरीर को मैंने भेड़िया पुजारी की गिरफ्त में पाया। उसकी जकड़न से मुक्त होने की भरसक कोशिश की, बहुत छटपटाई, चीखी चिल्लाई, लेकिन उसकी गिरफ्त से छूट न पाई क्योंकि मैं तो ग्यारह वर्ष की बालिका थी और वो हट्टा-कट्टा मोटा-तगड़ा मर्द…!’’ इसी कहानी में वह अंतिम की पंक्तियों में सवाल करती नजर आती है कि ‘‘क्या मैं आखिरी देवदासी हो सकती हूँ?’’
यह महज प्रथा की भोगी हुई पीड़ा से उठाया गया वैयक्तिक सवाल भर नहीं, बल्कि प्रथा की सामाजिक मान्यताओं के ऐतिहासिक से लेकर आधुनिक चिंतन के परिप्रेक्ष्य में स्त्री के सभी आयामों को केंद्र में रखकर उठाया गया सवाल है कि क्या स्त्रियाँ धार्मिक या सामान्य सांस्कृतिक और सामाजिक अवधारणाओं के तहत सिर्फ यौन-शोषण का ही पर्याय हैं क्योंकि देवताओं से शादी करवाकर महंतों और मठाधीशों द्वारा किया गया उनका यह यौन-शोषण वास्तव में ‘वेश्यावृत्ति के रिफाइंड स्वरूप’ के अतिरिक्त और कुछ नहीं..कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि इस संकलन में उन्होंने स्त्री देह के राजनीतिक स्थल पर पितृसत्तात्मक सामंतवादियों की शोषणकारी सामाजिक समझ से निर्मित परंपराओं का ही विश्लेषण भर किया है, बल्कि परंपरा और प्रथा के नाम पर ऐतिहासिक साक्ष्यों और अद्यतन चिंतन के परिप्रेक्ष्य की चाक पर चढ़ते मानवीय इकाई के उस वृद्ध वर्ग को भी विश्लेषित किया है जो बर्बर युवा वर्ग की सामाजिक बर्बरता की भेंट चढ़ता आया है- संकलन में शामिल कहानी- ‘काशी-काशी ’ एक ऐसी ही कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने प्रथा के नाम पर दक्षिण की उस सामाजिक परंपरा को दर्शाया है जिसमें सामंतवादी बना युवा वर्ग बुजुर्ग होते मनुष्यों के जीवन को लील उनसे छुट्टी पाकर अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है। इस कहानी की पात्र संयुक्ता और उसकी सहेली के माध्यम से लेखिका ने तमिलनाडु के कुछ जिलों में आज भी जीवित ‘थलाई कूथल ’ नाम की उस क्रूरतम प्रथा को उजागर करने का साहस किया है जिसमें गरीबी का बहाना बताकर बुजुर्ग परिजनों की हत्या कर दी जाती है।
इस कहानी में उन्होंने बताया है कि कैसे कसाई युवा वर्ग प्रथा के नाम पर बुजुर्ग परिजनों की निर्मम हत्या के लिए उन्हें तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले उनके शरीर की तेल से खूब मालिश की जाती है। फिर ठंडे पानी से स्नान करवाकर उसे नारियल का पानी, तुलसी रस और दूध पिलाया जाता है। ये स्नेह और सेवा इसलिए ताकि तापमान इतना नीचे गिर जाए कि हृदयाघात का बहाना लगे और बुजुर्ग परिजन स्वयं ही स्वर्ग सिधार जाए, सबसे लज्जाजनक बात तो यह है कि इन सारी तथाकथित दर्शाई गई स्नेह और सेवा के बीच सभी नाते-रिश्तेदार उस समय काशी-काशी करते रहते हैं। शीर्षक कहानी ‘काशी-काशी’ को स्पष्ट करते हुए लेखिका बताती हैं कि ये काशी-काशी की रट इसलिए लगाए रहते हैं क्योंकि इनका मानना है कि काशी शिव की नगरी है और ऐसा जनमानस का विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा शिव धाम को जाने से मोक्ष को प्राप्त होती है। सच में कितनी अमानवीयता है इस दिखावे में कि इसकी जघन्यता हृदय को भेद जाती है। एक ओर तो ये काशी- काशी करते हैं और वहीं दूसरी ओर इस विधि से यदि बुजुर्ग की मृत्यु न हो पाए तो अन्य विधियों के द्वारा उस बुजुर्ग को मौत के घाट उतारने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन युवा कसाइयों के पास एक नहीं कुल 26 तरीके होते हैं बुजुर्ग परिजनों को जबरन मौत के घाट उतारने के।
मृत्यु की इन विधियों में व्याप्त सामाजिक मूल्यों के द्वंद्व का अतिरेक, घटते मानवीय मूल्य, बिफरती मानवता से खंडित होते समाज का स्पष्ट किंतु कितना मार्मिक चित्रण ही है कि पाठक की आँखें महज भर ही नहीं आतीं बल्कि हृदय का आक्रोश आँखों से पिघलने को आतुर हो उठता है। खंडित-चटकती मानवता से उपजे सामाजिक मूल्यों के द्वंद्वों के चित्रण का अतिरेक भाव यहाँ मुझे अनायास अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की स्थापना की याद दिला देते हैं। अरस्तु के सिद्धांत में उपस्थित यह विरेचन शब्द जिसका सीधा तात्पर्य शुद्धिकरण से है कि कैसे एक साहित्यकार समाज को संवेदनाओं की शाब्दिक-कला के माध्यम से परिष्कृत करता है। हालांकि सामान्य आलोचनाओं के सन्दर्भ में अरस्तु के इस सिद्धांत की कई अलग अलग व्याख्याएँ की गई हैं ,किंतु यहाँ इस संकलन के संदर्भ में मैं इसे सामाजिक परिष्करण से ही जोड़कर देख पा रही हूँ क्योंकि लेखिका की साहित्यिक संवेदनाओं की आतुरता सृजन के माध्यम से समाज को परिष्कृत करने की ओर ही उन्मुख है। इस संदर्भ में वह ‘पुनर्विवाह दंश’ में लिखती हैं- ‘‘पूर्णिया को इस विवाह से एक सुदृढ़ सहारा तो मिल गया किंतु मानसिक धरातल पर वह विक्षिप्त रहने लगी। समाज उसे हेय दृष्टि से देखता था। ’’
लेखिका के भीतर सामाजिक परिष्करण की यह चिंता संकलन में शामिल कहानी—‘सिसकती जिंदगी’ में भी देखने को मिलती है जहाँ उन्होंने सोशल मीडिया के बढ़ते दुष्प्रभाव से खंडित होते वैवाहिक जीवन को दर्शाते हुए नायिका कुमारिका के माध्यम से कहती हैं कि उसका पति मनमीत देर रात तक बिस्तर पर नहीं आता, कंप्यूटर पर बैठा, रात रात भर, ऑरकुट में लड़कियों से गन्दी-गन्दी चैटिंग करता रहता है। पत्नी के मना करने पर उसे मारता-पीटता है, वह भी तब जबकि दोनों का नेट के जरिए प्रेम विवाह है। एक ओर जहाँ ऐसे मुद्दों के माध्यम से लेखिका तकनीकी दौर के समसामयिक समाज के विखंडन से पाठकों के हृदय को स्पर्श करती नजर आती हैं तो वहीं दूसरी ओर परंपरागत-ऐतिहासिक-सांस्कृतिक खंडित मूल्यों का मार्मिक चित्रण भी बखूबी करती दिखती हैं।
लेखिका द्वारा प्रस्तुत समाज के मार्मिक चित्रण में पाठकों के आक्रोश का आँखों से पिघलकर बाहर आना, यह सिर्फ स्पष्ट प्रस्तुति नहीं बल्कि लेखकीय चित्रात्मक शैली की प्रस्तुति है जिससे पाठक कहानी की मूल संवेदनाओं से स्वयं को आसानी से जोड़ पाते हैं। सत्य है,किसी भी सृजन की सफलता उसकी चित्रात्मकता पर निर्भर करती है कि वह अपनी इस शैली में पाठकों पर कितना प्रभाव डाल पाते हैं। इस संदर्भ में आदि कवि वाल्मीकि की पंक्तियाँ याद आती हैं कि ‘‘या निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती समा/ यत् क्रौंच मिथुनार्दकम अवधी काममोहितम्’’ क्रौंच पक्षी के वध से हुई सघन वेदना हमें महसूस नहीं हो पाती यदि कवि ने इन पंक्तियों में वध के साथ बाण की गूँज और क्रौंच पक्षी की चीख की अनुभूतियों को यूँ संवेदनशील पंक्तियों में आबद्ध न किया होता। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं लेखिका की शैली की तुलना आदि कवि वाल्मीकि से करने का दुस्साहस कर रही हूँ। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ संदर्भगत इन पंक्तियों के स्मरण के माध्यम से मैं सृजकों की शाब्दिक चित्रकला-शैली की बात करना चाह रही हूँ जिसका सीधा प्रभाव पाठकों के हृदय पर पड़ता है।
चित्रात्मकता के प्रति लेखिका का चौकन्नापन तब और भी उभर कर सामने आता है जब पाठक पुस्तक के आवरण को ध्यानपूर्वक देखता है। जो महज सुंदर ही नहीं बल्कि रंगों के माध्यम से एक ओर जहाँ स्त्री के भीतर का खंडन स्पष्ट हो रहा होता है तो वहीं दूसरी ओर अपने भीतर की ज्वलन के बीच उसके तटस्थ और संकल्पित निर्णय के तटस्थ भाव भी स्पष्ट हो रहे दिखते हैं। चित्रात्मकता के संदर्भ में, आखिरी देवदासी कहानी हो या खंडित यक्षिणी- उनमें उल्लेखित हृदय और परिस्थितिजन्य वाक्य-संवाद सभी में कहीं-न-कहीं लेखिका द्वारा किये गए चित्रात्मक अभिव्यक्ति के प्रयास की ही देन है कि वे सीधे से पाठक के हृदय को छू पाते हैं। चाहे वह ‘आखिरी देवदासी ’और ‘खंडित यक्षिणी ’ की स्त्री चीख हो या फिर ‘काशी- काशी’ की क्रूरतम प्रथा की जघन्यता या फिर ‘पिता की ममता ’, ‘सिसकती जिंदगी’ में उल्लेखित परिवेश ही क्यों न हो लेखिका पाठक को इनसे जोड़ पाती हैं। परिवेश और परिस्थितियों को चुनने में लेखिका ने तत्सम शब्दों के प्रयोग से बचते हुए जिन सरल संवादों और भाषा शैली का प्रयोग किया है वह उन्हें आम पाठकों तक सीधे से पहुँचाती है।
‘पुनर्विवाह दंश’, ‘नेकी कर दरिया में डाल’, ‘अर्थी सुसंस्कारों की’ जैसी संकलन में शामिल कहानियों के माध्यम से लेखिका ने समसामयिक-सामाजिक मुद्दे को सीधे-सीधे रखने का सफल प्रयास किया है। परिवर्तनकारी विचारों या सामाजिक बदलाव के लिए आतुरता से विचरता लेखिका का मन पात्रों की इच्छा शक्ति के माध्यम से वैयक्तिक और सामाजिक चिंतन की सजग किंतु सहज अभिव्यक्ति तो करता है, किंतु परिवेश और परिस्थितियों की इस बुनावट में हुई बारीक-बारीक चूक सजग पाठकों को कहीं थोड़ी सी खटकती भी है और वे एक ओर जहाँ लेखिका की खुली दृष्टि से जुड़ते नजर आते हैं तो वहीं दूसरी ओर खंडित यक्षिणी और देवदासी के अतिरिक्त शामिल कहानियों में परिवेशीय और परिस्थितियों का खुलकर किए गए वर्णन की प्रतीक्षा भी करते दिखते हैं।
हालांकि,लेखिका ने सामाजिक-सांस्कृतिक-ऐतिहासिक और पारंपरिक द्वंद्वों को लिखने के क्रम में अपनी दृष्टि खुली और चौकन्नी रखी है, किंतु शिल्प और अंतर्वस्तु के तहत कहीं-कहीं टकराती ये कहानियाँ पाठकों के पाठकीय प्रवाह को रोक देती हैं और वे रुककर, पन्नों को उलट पुलट कर पुनः पाठकीय स्वाद में इस उम्मीद से लौटने की कोशिश करते हैं कि अपने अगले संकलन में लेखिका इसकी भरपाई ज़रूर कर लेंगी। साथ ही, पाठक यह भी उम्मीद करते हैं कि विषय की समझ से परिपक्व इन कहानियों के कहीं-कहीं ठहराव और पकने की जरूरत शेष रह गई है उसकी भरपाई भी लेखिका अगले संकलन के माध्यम से करेंगी और पाठकों को अगली बार खूब तरीके से गहरी- पकी हुई कहानियाँ पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें जरूरी जगहों पर ठहर कर, उनकी खूब कसी बुनावट कर, पात्रों और परिवेश को प्रस्तुत करते हुए लेखिका अधिक परिपक्वता से कहानियों को पकाकर पाठकों के आगे परोसेंगी। ताकि जिस तरह यह संकलन, समाज के यथार्थ में व्याप्त खंडित मूल्यों को प्रतीकात्मक रूप से परोसते हुए पाठकों को अपनी संवेदनाओं से जोड़ पाता है वैसे ही आगे भी वे अपनी लेखकीय कृतियों के माध्यम से पाठकों को अपनी संवेदनाओं से जोड़ पाएंगी। मैं उन्हें खंडित यक्षिणी के लिए पुन: बधाई देती हूँ तथा आशा करती हूँ कि भविष्य में उनकी लेखनी ऐसे ही समृद्ध होती रहे।
प्रकाशक:
शब्दांकुर प्रकाशन
J- 2nd – 41,मदनगीर,
नई दिल्ली -110062
दूरभाष: 09811863500
मूल्य: ₹ 300/- (पेपरबैक)
$15/- (paperback)

समीक्षक- डॉ राशि सिन्हा
नवादा, बिहार