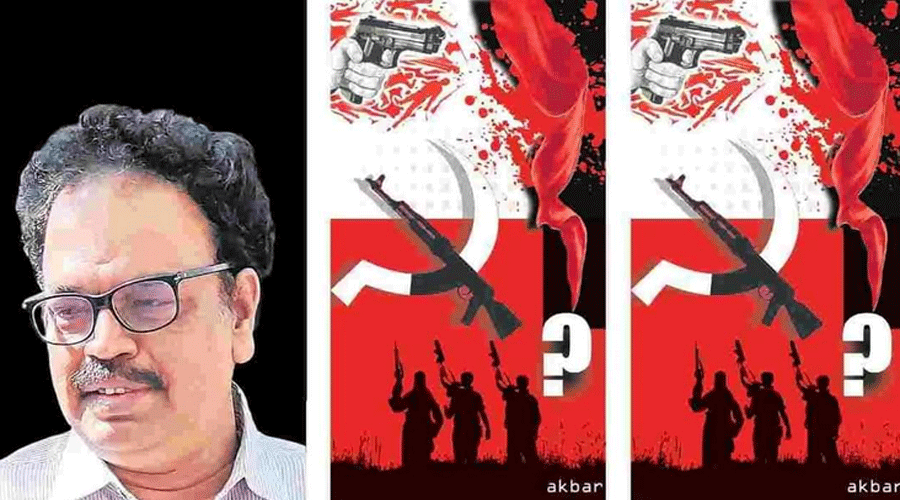मशहूर उर्दू पटकथा लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास ने 1980 में नक्सली फिल्म बनाई थी। फिल्म के अंत में भीषण गोलीबारी के बाद एक पुलिस अधिकारी एक मेगाफोन लेता है और चिल्लाता है, “क्या कोई नक्सली बचा है?” मौन ही जवाब होता है। लेकिन, दूर एक आदिवासी झोपड़ी में बिना कपड़े पहने एक लड़का दोनों हाथ उठाता है, जैसे वह है।
अब्बास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (वामपंथी) के प्रगतिशील आंदोलन के दौर से जुड़ा लेखक है। उसे नक्सली आंदोलन के प्रति पूरी तरह से कोई सहानुभूति नहीं है। और न ही कोई समझ है। उसे तो फिल्में बनाना भी नहीं आता। फिर भी फिल्म का अंत ऐसे क्यों किया होगा? उसता विश्वास है कि आंदोलनों को बलपूर्वक कुचला नहीं जा सकता है और अपेक्षा होगी कि आंदोलन जारी रहेंगे।
भारत के गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में माओवादियों के खात्मे की बात करते रहे हैं। 2026 की डेडलाइन बार-बार दोहरा रहे हैं। वे जैसे कह रहे हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ के गहनारण्ये अबूझमाड़ में दल के दल और गांव के गांव लोग मर रहे हैं। सरकार को उस मौत में सफलता दिख रही है। कटे हुए सिरों और काटे जाने वाले सिरों की गिनती करके बता रहे हैं। इस आश्वासन की घोषणा कर रहे है कि सब कुछ जल्द ही समाप्त हो जाएगा। वे सपना देख रहे है कि चार हजार वर्ग किलोमीटर जंगल में नया विकास होगा।
नये समाज के निर्माण के लिए बंदूक थामे संघर्ष करने वाले ये नक्सल हमारे बीच साढ़े छह दशकों से दिखाई दे रहे हैं। ये सभी इसी समाज की कोख से जन्मे हैं। ये हमारे ही बच्चे हैं। उनकी रणनीति है कि बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा करना, आंदोलन करना और अंततः भारत (देश) पर कब्जा करना है। स्वाभाविक है कि सरकार और सिस्टम इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। नक्सल हथियारबंद होने और चोरी छिपे घुमने के कारण उन्हें मारना सरकारी पुलिस को बहुत आसान हो जाता है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ऐसे लोगों के मामले में कानून के मुताबिक चलना और जांच करना अनावश्यक है। नतीजा यह हुआ कि हजारों नक्सली खत्म हो गये। साथ ही हजारों नये नक्सलियों ने भी जन्म लिया। अब सरकार इस बात का आनंद ले रही है कि इस पुनरावृत्ति प्रक्रिया में नक्सल को खात्मा करने में सफलता मिली है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
दरअसल, सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत नक्सलियों से ही नहीं हुई। उससे पहले कम्युनिस्टों ने किया था। उन्होंने तेलंगाना सहित देश के कई हिस्सों में बंदूक थामे संघर्ष किया है। उनसे पहले भगत सिंह और अल्लूरी सीतारामराजू जैसे क्रांतिकारियों ने हथियार उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हैं। 1857 में भारतीय किसानों और सैनिकों ने विद्रोह किया और संघर्ष किया तथा हार गये। हालाँकि, उसके बाद भी अनेक तरह से संघर्ष जन्म लेते ही जा रहे हैं। आजादी के बाद भी कई जगहों पर कम्युनिस्टों और गैर-नक्सलियों ने भी सशस्त्र संघर्ष किया और कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कई हथियारबंद संगठन सक्रिय हैं। सरकार उनमें से कुछ के साथ बातचीत कर रही है और समझौते भी कर रही हैं। जहाँ समझौते हुए, वहाँ कुछ विद्रोहियों ने उसे स्वीकार नहीं किया और आज भी लड़ रहे है। संस्थाएँ लुप्त हो सकती हैं, कुछ स्थानों पर संघर्ष मौन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे समाप्त हो जाएँगे।
हम तर्क सुनते हैं कि कोलंबिया में गुरिल्ला आंदोलन माफिया में बदल गया है और अंततः आत्मसमर्पण कर दिया है। श्रीलंका में टाइगर्स का सफाया हो गया है। हमारे देश में खालिस्तान आंदोलन कम हो गया है और नेपाल में माओवादियों का सफाया हो गया है। उपरोक्त उदाहरणों में कहीं पर भी समस्या शेष रुका नहीं है। नये-नये रूपों में अशांति प्रकट हो रही है। ऐतिहासिक स्मृति के रूप में भी संबंधित आंदोलन वर्तमान राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि जिस कारण वहां सशस्त्र संघर्ष किये गये उसके मूल कारण समाप्त नहीं हुए हैं। जहां कोई समस्या नहीं थी, वहां यह केवल दोनों पक्षों की सहमति और जुझारू लोगों की मांगों की पर्याप्त पूर्ति के साथ हुआ है।
1990 के दशक की शुरुआत में, जब सोवियत संघ का पतन हुआ, तो पूंजीवादी दुनिया ने खुलेआम जश्न मनाया। हालांकि बुद्धिजीवियों ने कहा कि इतिहास ख़त्म हो गया है। तभी एक अंतरराष्ट्रीय पत्रकार ने अपने कॉलम में कुछ व्यंग्यात्मक ढंग से सवाल पूछा, “लेकिन क्या हुआ? क्या लोग दुनिया में उनके पास जो कुछ है उससे संतुष्ट हो जाएंगे? क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि पूंजीवाद सर्वोत्तम है और इससे बेहतर कोई व्यवस्था नहीं है? क्या वे अपनी सरकारों और अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका में सरकारों पर शासन करने वाली महाशक्तियों का विरोध करना बंद कर देंगे और हमेशा के लिए खुशी से रहेंगे?”
इस सदी के पहले दशक में 11 सितंबर, 2001 की महत्वपूर्ण घटना के बाद दुनिया भर में हवाई यात्रा प्रतिबंधित कर दी गई थी। हवाई अड्डों को किले में तब्दील कर दिया गया था। इसके बाद लंदन में मेट्रो में आतंकी विस्फोट हुआ। इस पर टिप्पणी करते हुए एक अन्य पत्रकार ने दिलचस्प विश्लेषण किया। यदि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर विमान हमले अंतर्निहित कारणों पर केंद्रित किये बिना, यदि और अधिक लोगों को आतंकवादी रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रतिशोधात्मक उपाय किए जाते हैं तो सुरक्षा कैसे संभव है? यदि आप विमानों को रोकेंगे तो आत्मघाती हमलावर रुक जायेंगे। लेकिन, विस्फोट कहीं और शुरू हो जाएंगे। विश्लेषण का सारांश यह है कि सुरक्षा उपायों का समाधान हमेशा राजद्रोह की जगह और तरीका बदल सकता है, लेकिन यह राजद्रोह को नहीं रोक सकता है। जब अशांति होती है तो उसके दुष्परिणाम सामने आते रहते हैं। यदि एक रूप मिट जाता है तो वह अन्यत्र, दूसरे रूप में प्रकट होता रहता है। किसी चीज़ को मौलिक रूप से उखाड़ने के लिए, सबसे पहले यह जानना होगा कि बीज कहाँ है, कौन-सी मिट्टी अंकुरों को क्यों जन्म दे रही है और इसकी जड़े कहाँ तक फैली हैं और कितनी गहराई तक फैले हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि मिट्टी में कौन सी जैव रासायनिक गतिविधि उन पौधों को जीवित रख रही है।
अब, जैसा कि गृहमंत्री अमित शाह के अनुसार, मान लीजिए कि वैसे हर कोई पकड़ा जाता है, आत्मसमर्पण करता है और मर जाता है। आगे क्या होता है? 370 के निरस्त होने के लिए कश्मीरी तरस रहे थे, तो क्या जन्मधन्य महसूस करने वाले पीएम मोदी ने जो चाहा वैसे हो गया है। क्या देश के सभी आदिवासी उस आनंद में डूब गये है? उनके (सरकार) और विकास के बीच बाधा बनकर खड़े क्रांतिकारियों का अंत हो गया मानकर क्या जश्न मनाएंगे। वनवासी कल्याण हुआ मानकर अडानी-अंबानी के साथ मौजमस्ती करके जीवन बिताएंगे? अंग्रेज वाले भी नहीं पहुंच पाने वाले ऐसे भयंकर जंगल के बीच से कईं मार्ग तेजी से हो रहे नागरिक विकास को देखकर क्या वे प्रफुल्लित हो जाएंगे? क्या माओवादियों की गोलियों की आवाज़ ठंड होकर और युद्ध आर्ट प्रशिक्षण की आवाज़ के साथ दंडकारण्य (घना जंगल) नए वसंत का अनुभव कर पाएगा?
न केवल जंगलों में रहने वाले आदिवासी, बल्कि उस अन्ना (नक्सल) को याद करने वाल ग्रामीण प्रजा, अधिकार और न्याय जैसे बीत चुके पुराने शब्दों को बोलने वाले आम आंदोलनकारी और स्वीकार न किए जाने पर भी अपना सम्मान नहीं खोने वाले बुद्धिजीवी इन सबका क्या होगा? तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष से शुरुआत करके लगभग सात दशकों तक आंदोलनकारियों को समाप्त करते आई कांग्रेस पार्टी को भी अब शहरी नक्सलियों की छाप से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो देश में माओवादी का ठप्पा लगने वाले कौन बच पाएंगे? अमित शाह जी ये सब रहते हुए अंत कैसे संभव है? अबूझमाड़ के बाद, कई युद्धक्षेत्र हैं! जब कोई उन्मूलन करने वाला ही नहीं है तो वास्तविक शासन कैसे कार्य कर सकता है? उन महाशक्तियों का समय कैसे बीतेगा जो कभी भी और कहीं भी युद्ध नहीं होता है और हमेशा किसी न किसी का विनाश देखने वाले कल की महाशक्तियाँ क्या चैन से बैठ पाएंगी?
शायद, शारीरिक रूप से अबूझमाड़ को ‘मुक्ति’ मिल जाएगी। जनतन सरकार यादगार बन जायेगी। देश में इधर-उधर माओवादी आंदोलन केंद्र भी गंभीर दबाव में दब जायेंगे। जब अंत की घोषणा और कार्यान्वयन किया जाता है, तो निराशाजनक अंत होना वीरतापूर्ण हो सकता है, लेकिन यह सही नहीं हो सकता है। जब समय तेजी से आगे बढता है या उत्साहित होता है, तो आलोचना को आमंत्रित करने की विनम्रता और समीक्षा करने की आवश्यकता की कमी हो सकती है। प्रतिबंध और उन्मूलन के सामने आलोचना और समीक्षा अनुचित और कायरतापूर्ण लग सकती है। फिर कैसे अपने आपको बचाव करने के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक विफलता से पीड़ित हो रहे लोगों को सहयोग और समर्थन करने के लिए कौन बच पाएंगे? जन-जीवन में उत्पन्न होने वाले अनेक युद्धक्षेत्रों का प्रबंधन कौन कर सकता है? शासकों के अनुसार जबरदस्ती से उन्मूलन संभव नहीं है। ऐसे में विवेचन और आलोचना की कमी होने पर लोग चाहेंगे कि माओवादी से बात की जाये।
उन्मूलन लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही कदमों को रोकने के लिए विज्ञप्तियों को सुनने की स्थिति में सरकार नहीं है। दरअसल, भारतीय नागरिक समाज और जन आंदोलन ऐसी अपील करने की स्थिति में भी नहीं हैं। मुख्यधारा की पार्टियाँ चुपचाप आधी-अधूरी सहमति दे रही हैं। केवल कहने और सुनने वाले कोई है तो वह माओवादी ही है। कोई भी अस्त्रसंन्यास करने को नहीं कहता है। केवल कोई भी यह पूछ सकता है कि अन्यायपूर्वक नष्ट न हो जाये
के. श्रीनिवास संपादक तेलुगु दैनिक आंध्रज्योति