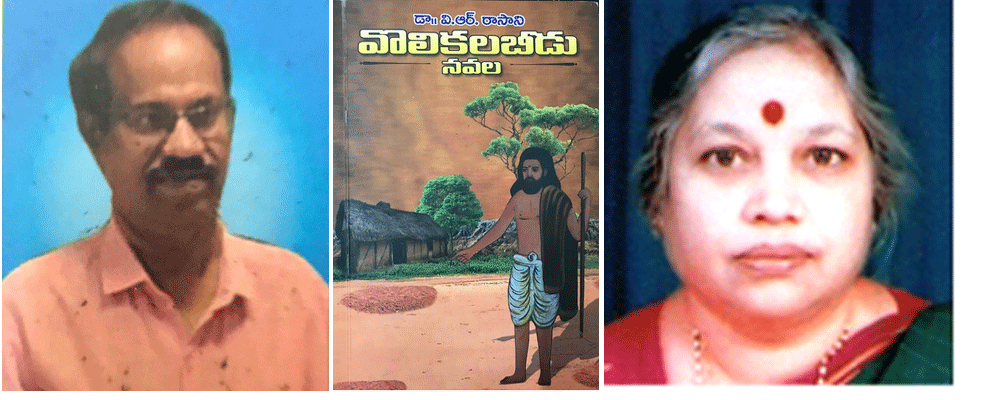तेलुगु में श्मशान को ‘वोलिकलबीडु’ कहते हैं, जिसकी देखरेख विशेष मसानियाँ या डोम लोग करते हैं। ये डोम जीवन की सच्चाई के इतने क़रीब जीते-से लगते हैं कि साधारण मनुष्यों की मुख्य धारा से छूटे गोचर होते हैं। यह इसलिए कि आम मनुष्य भी उनसे उतनी ही दूरी इस मानसिकता से बनाए रखते हैं, मानो वे प्रेतों के बीच निवास करते-करते कुछ वैसे ही बन गए हों… उनका हुलिया भी तो ऐसा, जैसा कि वहाँ एकांत में किसी का उनसे आमना-सामना हो जाए, तो भय की एक लहर शरीर पार कर जाए…
एक माँ की ‘कोख’ में प्राणी को शरीर मिलता है, तो उसके वय की पूर्ति के बाद उसके शरीर को समाप्त होना होता है श्मशान की भूमि (खोक) में… जहाँ माँ प्रसव श्रम से शिशु को प्राण देकर अपनी कोख से जन्म देती है, वहीं डोम श्रम से प्राण छूटे व्यक्ति के शरीर (शव) को भू-भाग ‘खोक’ में समा देता है।
आगे चलकर हर मृतक के लिए कुछ नई कहावतें बनेंगी- ‘कोख से आया खोक में गया’, ‘कोख से खोक तक’, ‘अंत में खोक में ही तो समाना होता है’… आदि।
यह भी पढ़ें-
शवों की अंतिम क्रिया संपन्न करना डोम लोगों का पारिवारिक पेशा है। उनकी पीढ़ी-दर-पीढ़ी श्मशान से जुटी रह जाती है। वेतन भी इतना नहीं पाते हैं कि बच्चों को पढ़ा-लिखा सकें। एक अनपढ़ के लिए यह स्वयं वृत्ति बन गई है। गाँवों-जिलों में हर मरघट पर एक डोम परिवार अपना दायित्व निभाता दिखाई देता है। शहरों में भी पहले यही बात थी, पर अब म्युनिसिपैलिटी ने अपना विधान बनाकर डोमों के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया…
श्मशान एवं डोमों का सही चित्रण डॉ. वी. आर. रासानी जी के इस ‘वोलिकलबीडु’ पुस्तक में गोचर होता है। एक डोम को अपने और परिवार के गुज़ारे के लिए मरघट पर अपना दायित्व निभाने के साथ-साथ और जाने क्या-क्या करना पड़ता है… सड़कों पर मंत्र-तंत्र का व्यवसाय और यह भी उतनी कमाई नहीं दे पाता है कि वह साधारण मनुष्यों जैसे कोई छोटी वांछा पूरी कर सके… घर-घर माँगने भी जाते हैं, मुट्ठी भर चावल मिल गया तो बहुत है… बेबस-से रह जाते हैं, जैसे दरिद्रता से उनका नाता सदैव का हो…
तन-मन से समर्थ होते हुए भी डोमों का दरिद्रता से नाता तोड़ने का कोई भी यत्न सफल नहीं हो पाता है। यह इसलिए भी कि आम सामाजिक व्यवस्था इन्हें अपने से दूर रखती है।
तेलुगु पुस्तक तो पढ़ने को नहीं मिली, पर उसका डॉ. टी. सी. वसंता जी द्वारा हिन्दी अनुवाद ‘वोलिकलबीडु (मरघट)’ पढ़कर डोमों के जीवन से जुड़ी बहुत सी सच्चाइयाँ जानने को मिलीं। उनके वास्तविक जीवन कठिन, काँटों भरे पथ तो नहीं, पर फूलों वाले भी नहीं!
पता चला कि रासानी जी ने स्वयं जाकर डोम परिवार के साथ काफ़ी समय व्यतीत करके उनके जीवन की जानकारी ली है। कहा जाए तो उनकी यह कृति शोध-कार्य है।
डोम ‘दास’ बहुत ही मेहनती और दायित्व समझने वाला है। मानव हृदय रखता है, अत: बहुत ईमानदार है। उसकी पत्नी गंगी सही संगिनी है, उसके हर सुख-दु:ख में साथ निभाती है। पति की भावनाओं को समझकर अनुकूल व्यवहार करती प्रतीत होती है। उनका एकमात्र संतान है कासय्या। उनके तीन और बच्चे- सिन्नम्मी, बोंदय्या और भारप्पा। किन-किन हालातों में उन्हें मिले हैं, इस पुस्तक में विस्तार से बतलाया गया है। ये सब बच्चे गंगी और दास को हृदय से माँ-बाप मानते हैं और उनकी हर बात का आदर करते हैं। बड़े होते-होते ये तीनों बच्चे भूल जाते हैं कि वे कहाँ से आये और कौन थे- यही हैं डोम ‘दास’ के चरित्र को उजागर करने वाली बातें।
परिवार के ये सभी सदस्य ख़ामी में भी एकजुट रहकर मेहनत से घर चलाने की सोचते हैं… शव के आने में विलंब हो, तो दास अपने हाथ की सफ़ाई से सड़कों पर छोटे-छोटे जादुई कारनामें कर दिखलाता है। इस कार्य में परिवार के सभी सदस्य, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उसका भलीभाँति साथ देते हैं, कार्य सफल बनाते हैं। कभी-कभार भले घरों के गुसलखानों की सफ़ाई के लिए गंगी और सिन्नम्मी के निकल पड़ने की घटना भी है… इन सभी दृश्यों को लेखक ने बड़ी ही मार्मिकता से प्रदर्शित किया है।
सत्य हरिश्चंद्र की कथा से सभी डोम परिचित हैं। राजा हरिश्चंद्र ने अपना सबकुछ दान देकर अंत में वीरबाहु डोम बनकर श्मशान में अपना जीवन बिताया था। सभी डोम वीरबाहु को अपना आदर्श मानते हैं। श्मशानों के द्वारों पर ‘हरिश्चंद्र श्मशान’ का बोर्ड लगाए जाने पर डोमों ने आपत्ति जताई और कहा कि उस बोर्ड पर ‘वीरबाहु श्मशान’ होना चाहिए। पुस्तक के अनुसार इस वर्ण संबंधी विषय पर काफ़ी चर्चा चल रही है…
समय-समय पर दास एकांत में अपने जीवन का विश्लेषण करता गोचर होता है- उसने यह वृत्ति कैसे अपनायी; कैसे इसमें प्रवीणता पाई; कितना पाया कितना खोया; आगे का जीवन कैसा होने वाला है; वग़ैरह… वग़ैरह… उसने अन्य डोमों से मिलकर सरकार की दृष्टि अपनी ओर लाने का यत्न भी किया। आगे डोम अपना वृत्ति-धर्म किन स्थितियों में निभा पाएँगे? एक संदेह दास के मन में बैठा रह जाता है…
एक बात तो ध्यान देने योग्य है-
अलग-अलग धर्मों की अलग-अलग अंत्यक्रिया रीतियाँ… दो मुख्य तरीक़े- दफ़नाने और भस्म करने के… अलग-अलग समाजों की ये रीतियाँ भी भिन्न होती हैं। यही नहीं, एक ही वर्ण के भी अनुकूलता से रीतियाँ-आचरण बनाये गए हैं। परन्तु दफ़नाने की प्रक्रिया में भूमि का खाया-पिया मृतक अपना सबकुछ भूमि को लौटा जाता है। शरीर के भस्म होने पर ख़ाक में भूमि के लायक़ कुछ नहीं रह जाता है, नष्ट हो जाता है। कुछ भी जलाने पर एक तो व्यर्थ ख़ाक बच जाती है, दूसरा वायु प्रदूषण! हज़ारों वर्षों से इस प्रकार जलाने की प्रक्रिया के पीछे जो भी आस्तिक भावना रही हो, भूमि को कितनी हानि पहुँचाई गई है, अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता… ऐसा ही चलता रहा, तो एक दिन आएगा, भूमि के लिए साँस लेना मुश्किल हो जाएगा! वह दमे का शिकार बन बैठेगी… यह मात्र एक चेतावनी है, सावधानी बरतने की!
बहुआयामी साहित्यकार डॉ. वी. आर. रासानी जी की पहचान उनकी उनकी इन विधाओं में प्रस्तुत की गई रचनाओं से बख़ूब हो सकती है- २०० कथाएँ, १४ उपन्यास, २२ नाटक-नाटिकाएँ, ४०० शोध-आलेख, १०० से ऊपर की संख्या में कविताएँ एवं गीत… इनके हाथों वोलिकलबीडु जैसा उपन्यास लिखा जाना प्रशंसनीय है। इसमें जीवन से जुड़े अन्य विषयों से हटकर, न केवल श्मशानों की स्थिति एवं डोमों की जीवन-शैली का ज्ञान है, बल्कि हिजडा (किन्नर) जाति की प्रथाओं के भी विस्तृत दर्शन भी हैं।
इसी प्रकार बहुआयामी लेखिका-अनुवादक डॉ. टी. सी. वसंता जी की मौलिक एवं अनूदित कृतियों में प्रमुख हैं- तेलुगु साहित्य वटवृक्ष गुडिपाटि वेंकट चलम की ‘रमणी से रमणाश्रम तक’ १४०० पृष्ठों की तीन भागों में जीवनी; ‘मंटो ज़िन्दा है’ का तेलुगु अनुवाद; गीतकार गोपालदास नीरज पर शोध कार्य (पीएच. डी.) के साथ-साथ उन पर अनेकानेक आलेख और उपन्यास ‘विद्रोही वसुंधरा’ जैसी अनेक बहुचर्चित कृतियाँ।
दोनों साहित्यकारों के संयुक्त श्रम का नतीजा है यह उपन्यास ‘वोलिकलबीडु (मरघट)’। इस कार्य के लिए रासानी जी एवं वसंता जी को धन्यवाद और अभिनन्दन।
‘वोलिकलबीडु’ तेलुगु पुस्तक
लेखक- डॉ वी आर रासानी
‘खोक’ हिंदी पुस्तक
अनुवादक- डॉ टी सी वसंता

प्राक्कथन- देवा प्रसाद मयला
मोबाइन नंबर : 9849468604
ई मेल : devaprasadmyla@gmail.com