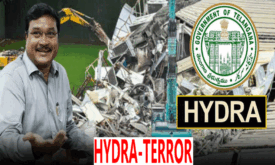समाचार पत्रों की दुनिया में यह नाम अछूता नहीं है। हां यह चंद्रमणि रघुवंशी की बात हो रही है। हाल ही में उनकी ‘समाज के सवाल’ नामक पुस्तक प्रकाशित हुई हैं। यह आपके विचार प्रधान लेखों का संग्रह है, जो निश्चित ही शोधार्थियों के लिए उपयोगी है। आपने संवेदनशील और अहम मुद्दों पर अपने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए करारा व्यंग्य कसा है। मानवता के नित्य प्रति हो रहे शरण पर भी गहरी दृष्टि रखते हुए अपने लेखों में संपादकीय धर्म का निष्पक्ष भाव से निर्वहन किया है। दैनंदिन जीवन के विभिन्न पक्षों का इन्होंने साक्षात्कार किया और उन पहलुओं पर चुनौतीपूर्ण समीक्षा की।
चंद्रमणि रघुवंशी संपादकीय क्षेत्र में एक सशक्त हस्ताक्षर है। उनकी साहित्य साधना 1975 से ही जारी है और कई साहित्यिक कृतियां प्रकाशित भी हुई। काव्य संग्रह कोख से सूरज की कारा तक और अंदर की आग और बर्फ का फूल (काव्य संग्रह) कतरा और समंदर (विचार संग्रह) है। इन्होंने पत्रकारिता की सतत सेवा 16 वर्ष की अवस्था से आरंभ कर दी यथा नई उम्र की नई फसल ‘हिंदी साप्ताहिक’ का स्वतंत्र संपादन ‘चिंगारी’ हिंदी साप्ताहिक तथा सांध्य दैनिक ‘बिजनौर टाइम्स’ हिंदी दैनिक का संपादन किया। इन्होंने कई समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें नवभारत टाइम्स (हिंदी दैनिक) हिंदुस्तान (हिंदी दैनिक) जनयुग (हिंदी दैनिक नई दिल्ली) नवजीवन (हिंदी दैनिक लखनऊ) ‘ब्लिट्ज’ तथा ‘करंट’ हिंदी साप्ताहिक बंबई का वर्षों तक प्रतिनिधित्व एवं ‘समाचार भारती’ यूथ सर्विस नई दिल्ली का वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया। संप्रति आप बिजनौर टाइम्स हिंदी दैनिक के संपादक है।
आधुनिक समाज के हर महत्वपूर्ण तत्वों को इन्होंने झिंझोड़ा है, तथा नए मूल्यों को संपादित करने ठोस कदम उठाने आह्वान किया है। सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलू पर भी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंथन किया है। चंद्रमणि ने अपने एक संपादकीय लेख ‘राम कहां है’ में उन अनुभूतियां पर कड़ा प्रहार किया है जिसका आघात व्यक्ति सह नहीं पाता जब चारों ओर से वह घिर जाता है कहीं राह नज़र नहीं आती, कोई ऐसा अपना नहीं दिखता जिसे वह अपना कह सके, मदद की गुहार लगा सके, मन की बात कह सके। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है तब उसे केवल ईश्वर ही सच्चा हितैषी जान पड़ता है और व्याकुल व्यथित मन राम को पुकारता है। पर राम भी तभी सुनते है या उनका हमारे साथ होने की अनुभूति तभी कराते हैं जब व्यक्ति विकारों, मनोविकारों से ऊपर उठकर उनका त्याग करता है।
यह भी पढ़ें-
“घंटे की खोज के बाद मेरे सामने भूख, तृष्णा, पिपासा अपने लंबे-लंबे हाथ फैलाए आ खड़ी होती है। आंखें बंद है फिर भी मैं उनकी उपस्थिति का आभास करता हूं। मैं उनसे पूछता हूं राम कहां है? और वे अट्टहास करती हैं– राम को हमारी उपस्थिति में खोज रहे हो? हमारी उपस्थिति का अहसास ‘शून्य’ कर दो तो राम मिले।” यह कैसा संभव है? मेरा मन प्रश्न करता है और तब मेरी आत्मा बोल उठती है, तृष्णा, भूख, पिपासा का शरीर से संबंध है आत्मा से नहीं।” (राम कहां है–पृ.सं 12)
सच ही तो कहा है कि भूख प्यास तृष्णा पिपासा का संबंध शरीर से होता है और शरीर का संबंध सांसों से होता है। जब आत्मा देह छोड़ती है तो उसका संबंध शरीर से छूट जाता है, शरीर निर्जीव हो जाता है मानवीय तृष्णाएं अब उसे नहीं सताती जब तक भूख प्यास तृष्णा शरीर को घेरे रहती है, राम का नाम कहां कोई ले पाता है। ज़िंदगी की आपाधापी और तृष्णाओं में ही उलझ कर रह जाता है। वे कभी तृप्त नहीं होती। मनुष्य को व्याकुल करती रहती है। राम नाम का सुमिरन यदि कर भी ले तो वो आध्यात्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत नहीं होती , निसार जीवन की विडंबना यही है कि पहले इन्हें शांत करना पड़ता है। इसके लिए बड़े त्याग करने पड़ते हैं जो अत्यंत कठिन है। जो इन सब से ऊपर उठ गया वही सच्चे हृदय से राम के नाम का सुमिरन कर पाता है। “मुझे लगता है कि दृश्य और चेतावनियाँ जब आदत में शामिल हो जाती हैं तो अपना महत्व खो देती हैं खासतौर से ऐसी चेतावनियां जिन्हें केवल खानापूर्ति के उद्देश्य से प्रदर्शित किया गया हो देर तक अपना प्रभाव बनाए रखने के योग्य नहीं होती है।” (एक पैकेट सिगरेट और चेतावनी पृ.सं–41)
मनुष्य आदतों के वशीभूत हो जाता है। जब वह दृश्य चेतावनियों को पढ़कर भी एक पल एक दिन के लिए डरता तो है पर आदत के आगे वे सब निरर्थक जान पड़ती हैं। वह अनुभूत करता है कि इससे उसे मर्मांतक पीड़ा होगी पर फिर भी अपनी आदतों में परिवर्तन लाना उसे बेचैन करती है और वह इन चेतावनियों को नजर अंदाज करता चला जाता है। उसकी मनोदशा उसे व्यथित करती हैं कि एक छोटे सिगार के पैकेट पर जो कि सिगरेट पीना उसकी आदत है, चेतावनी छोटे अक्षरों में लिखी होती हैं पहली बार पढ़कर डरना सहमना और फिर उसे नजर अंदाज करना आदत के वशीभूत होना है। इन हानिकारक वस्तुओं को बनाने वाले स्वास्थ्य के प्रति छोटे अक्षरों में चेतावनी लिखना अपने कर्म की इतिश्री समझते हैं और धड़ल्ले से ये सब चीजें बेचते हैं। उपभोक्ता चेतावनी को नजर अंदाज करने में ही अपनी आदत की भलाई समझता हैं। मानव मूल्यों के क्षरण की अति यही तो है।
जब कोई नहीं सुनता मनुष्य सब और से थक हार जाता है। सारे रास्ते बंद नजर आते हैं कहीं से कोई सहयोग न मिले तब वह ईश्वर को मदद के लिए पुकारता है। सारे जंजालों से मुक्ति का रास्ता जब कहीं नजर नहीं आता। आहत हृदय दुनिया से विमुख ईश्वर की शरण में जाता है। उसे यही वह ठोर ठिकाना नज़र आती है जहां वो दुख, संताप को हरने की गुहार लगा सकता है। इस भरोसे से की ईश्वर उन सब से उसे मुक्ति अवश्य दिलाएंगे।
“तुम्हारी जेब खाली थी और तुम्हारी पत्नी ताने दे रही थी अगर बच्चों की जिद पूरी नहीं कर सकते तो बच्चे तुमने पैदा ही क्यों किए थे। और इस ताने के बाण तुम्हारा हृदय को विदीर्ण करते चले गए थे। तुम अपनी व्यथा सुनाने के लिए अपने मंदिर में चले गए।” (भागकर कहां जा रहे हो–पृ.सं. 88)
जब मुसीबत चारों ओर से घेर लेती है। आर्थिक स्थिति डांवाडोल होती है खाली जेब होती है और मन व्यथित होता है। ऐसे में यदि बच्चे किसी चीज़ की जिद पकड़ ले और वह पूरी न कर पाए तो उसका मन बहुत व्यथित हो जाता है। ऐसे समय में पत्नी उन्हें समझाने के बजाय पति को ही उलाहना देती हैं कि जब जेब खाली थी तो बच्चे पैदा क्यों किए। वह इन शब्द बाणों को झेल नहीं पाता, क्या बच्चे सिर्फ उसकी ही इच्छा थी, उसी का फैसला था, क्या पत्नी का कोई सहयोग नहीं था। आज उसके पास पैसा नहीं है तो पत्नी भी कटाक्ष करने लगी। प्यार का अंकन यही है कि मुसीबत में जीवनपथ पर समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति जीवन संगिनी और उसके बीच खाली जेब आ गई। यह जिंदगी का कटु सत्य है जिस पर चंद्रमणि ने गहरा कटाक्ष किया है। आगे व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि विदीर्ण हृदय अपनी व्यथा किसे कहे और वह अपनी व्यथा सुनाने मंदिर चला जाता है। उसको समझने वाला कोई नहीं, शायद भगवान उसकी बात समझ सके। उसे ईश्वर के सिवा उसका अपना कोई नज़र नहीं आता। भागकर जाए तो कहां जाए। बाहरी दुनिया अब उसे उसके काबिल नहीं लगती और वह अपनी व्यथा सुनाने मंदिर में भागता है। वहीं अपनी पीड़ा को हरने की गुहार लगाता है।
“जब व्यक्ति बंधनों से ऊपर उठ जाए, संबंधों की जकड़ से मुक्त हो जाए और जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के रहस्य को समझ जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाना बहुत बड़ी बात है यह आसान काम नहीं है। लेकिन हम प्रारंभ कर सकते हैं सबसे पहले क्रोध को त्याग कर। क्रोध का त्याग बेहद कठिन है और क्रोध को त्याग कर ही स्थिति प्रज्ञ हुआ जाता है।” (आश्रम में शांति की खोज पृ.सं 16)
मनुष्य कहीं भी घूमने चला जाए मंदिर चला जाए या कहीं आश्रम में चला जाए वह शांति की तलाश में कहीं भी चला जाए, उसे शांति नहीं मिलती जब तक कि वह स्वयं के भीतर के उद्वेलन को शांत नहीं करता। उसे शांति बाहर से नहीं भीतर से मिलेगी। संबंध ही तो है जो व्यक्ति को जरूरत और तकलीफ में काम आते हैं वहीं कभी-कभी जरूरत तकलीफ और दुख में जब हमारे सारे संबंध हमसे मुख मोड़ लेते हैं तब हमारे अस्तित्व पर सबसे गहरा प्रहार होता है। ऐसे समय में ही सच्चे और झूठे संबंधों का व्यक्ति को बोध होता है,वह संबंधों से ऊपर उठना चाहता है जिन संबंधों से अब तक वह जकड़ा हुआ था उसे अब वह बेजान व निरर्थक जान पडते हैं। वह उनसे मुक्त होना चाहता है। उसके दिल की गहरी चोट उसे संबंधों से विमुख करती है। स्थिति का भान होने पर उसे उन परिस्थितियों से लडना पड़ता है। विनम्रतापूर्वक बिना क्रोध किए, बिना क्रोध जताए। वह उन्हें छोड़ देना चाहता है तो कभी वह उनसे बदला लेने की ठान लेता है। सत और असत के अंतर्द्वंद्व की विभीषिका में जलता है। यदि संबंधों से ऊपर उठना है तो, व्यक्ति को खुद के भीतर के अस्तित्व को पहचानना जरूरी है और जब ऐसा होता है तब वह स्थिति को बखूबी संभाल सकता है। संबंधों से दूर भागने के लिए सर्वप्रथम क्रोध को त्याग करना होता है। लेकिन मानवीय भावनाएं अहं, क्रोध, जलन, ईर्ष्या जैसे विकारों पर क्या विजय पाना इतना आसान है। स्वयं को समेटना पडता है। इतना आसान नहीं होता है सारे संबंधों से ऊपर उठकर स्वयं को स्वयं में समेटना, खुद में सिमट कर ही मनुष्य अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता की खोज कर सकता है। अंतर्मन की विभीषिका में जलते हुए व्याकुल मन को शांति में भिगोते हुए जब वह स्थिति से पूरी तरह से रूबरू होता है तब कहीं उसे अपने मूल्य का बोध होता है। जीवनासक्ति का अंत यही होता है और उसके अस्तित्व का निर्माण होता है।
चंद्रमणि ने अपने एक संपादकीय लेख ‘दीप और मैं’ में लिखा है –
“अंधेरे की गहरी साजिश के खिलाफ जलता हुआ दीप,
खुद जलता हुआ दूसरों को रोशनी देता हुआ दीप,
लेकिन क्या दीप ही जलता है
जलती तो और भी चीजें हैं पर क्या वे तन को विदीर्ण करती है
जल तो मैं भी रहा हूं पर रोशनी कहां है
मैं अपने अंदर उठती हुई लपलपाती लपटों, ऊंची अग्नि शिखा को महसूस कर रहा हूं लेकिन इनमें तो रोशनी नहीं है और न आंच है इन घनघोर अंधेरे में खुद भटक रहा हूं रास्ता खोज रहा हूं जब रोशनी नहीं तब क्या जरूरत है तिल – तिल जलने की?”(दीप और मैं–पृ.सं. 107)
“अंधेरे के खिलाफ लड़ने के लिए जरूरी है हौंसले, विश्वास, क्षमता और ऊर्जा की।” (दीप और मैं–पृ.सं. 108)
अंधेरे में दीप की रोशनी का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि दीप खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है और चंद्रमणि कहते हैं कि क्या केवल दीप ही चलता है।शरीर को जो विदीर्ण करे ऐसी बहुत सी चीजें होती है। मनुष्य भी दुनिया,परिवार रिश्तों और अपनों द्वारा दिए गए जख्मों की मर्मांतक पीड़ा सहता है। वह किसी से कह नहीं सकता। उसके स्वयं के भीतर ही एक अजीब सी अग्निशिखा जलती है उस जलन की उष्णता को वह भीतर ही भीतर महसूस तो करता है। परंतु उसकी अभिव्यंजना वह किसी से नहीं कर पाता जो उसे भीतरी ही भीतर जलाती है। उसका इस तरह जलना प्रकाश नहीं देता, न ही वहां ऐसा कोई प्रकाशपुंज होता है, जो मन के भीतर के अंधेरे को खत्म करे उसकी जलन को चंदन का लेप करे।
चंद्रमणि त्रिपाठी ने अपने विविध लेखों द्वारा पाठकों का ध्यान खींचते हुए जीवन, समाज, भौतिक जगत, भ्रष्टाचार, उपभोक्तावादी संस्कृति पर उन्हें सामाजिक सवालों का दर्पण दिखाया है। उनकी समीक्षापरक लेखनी उनके विचारों की गहराई का ही बोध नहीं कराती बल्कि यही सवाल सोचने को मजबूर करते हैं। यही समाज के सवाल हमारे मन मस्तिष्क को मथते हैं। आपके विचार प्रधान लेख समाज के यथार्थ का साक्षात प्रतिबिंब है। संवाद करते संपादकीय लेख बाह्य और आंतरिक जगत में फैले कालुष्य पर सवालों के कटाक्ष, निश्चित ही शोधार्थियों में नई सोच के अंकुर को नव प्रस्फुटन देते हुए नई पौध को सोचने जमीनी सच्चाई जानने और इन सवालों का जवाब खोजने पर मजबूर करेंगे।

समीक्षक : डॉ.संगीता शर्मा
4-7-156/193rd floor
छोटा शिव हनुमान मंदिर
भानोदया हाई स्कूल के पास
पांडुरंगा नगर
अत्तापुर – हैदराबाद – 500048
तेलंगाना
Sangeeta.dr3101@gmail.com
M. No. 8096547310
पुस्तक : समाज के सवाल
लेखक : चंद्रमणि रघुवंशी
प्रकाशक : हिंदी साहित्य निकेतन
बिजनौर (उ.प्र)
प्रथम संस्करण 2024
पृष्ठ : 112
मूल्य : दो सौ पचास रुपए।